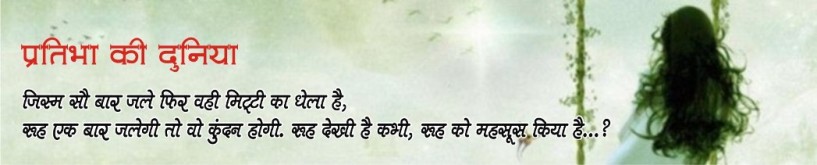'आप न तो मेरी नानी की बेटी हो, न मम्मा की बहन तो फिर मेरी मौसी कैसे हुई?' प्यारे से अनि से मेरी दोस्ती की शुरुआत उसके इसी सवाल के साथ हुई थी. मेरा पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अब अपने सवाल से खाली था. धीरे-धीरे दोस्ती गहराने लगी, पहले पहल वाली झिझक, संकोच अपनी गठरी बाँध के चलता बना. देवयानी को मैगी और ऑमलेट बनाने किचन की ओर भेजकर हम बिंदास मस्ती करते. चादर तानकर टेंट बनाने का मजा, आहा. बच्चा हुए बिना बचपन का आनंद ले पाना असंभव है, ये राज़ मैं जानती थी. मेरे भीतर का बच्चा मौका पाते ही उछलकर बाहर आने को बेताब रहता ही है. अनि का हाथ थामते ही वो बाहर आ गया.
मैं और अनि खूब मस्ती करते. उस रोज छुट्टी का दिन था और हमने टेंट बनाने की योजना बनाई. ज़ाहिर है देवयानी के कमरे का हाल तो बुरा होने ही वाला था लेकिन हम दोनों मूड में आ चुके थे. टेंट बनाने का सामान अनि ने जुगाड़ना शुरू किया.
हमारा टेंट एक तरफ से बनता तो दूसरी तरफ से गिरने लगता. योजना यह थी कि नाश्ता टेंट में ही होगा. इतने में देवयानी की आवाज आती कि 'चलो उठो, नहाओ तुम दोनो, फिर चलना भी है...' हम दुबक जाते, सोचते कि कैसे न जाने का जुगाड़ बिठाया जाये ताकि सारा दिन खेला जा सके. अनि कहता ' मासी काश कहीं से फोन आ जाये कि जहाँ जाना था वहां का प्रोग्राम कैंसिल हो गया .' उसकी इस बात पे उसे खुद ही हंसी आ जाती और हम दोनों मुंह दबाकर हँसते.
बहरहाल टेंट बनकर ही रहा और हमने नाश्ता टेंट में ही किया. इस दौरान अनि ने पूरे फौजी ढंग से टेंट बनाने में अपनी भूमिका निभाई. जैसे ही मैंने कहा, 'देखो, दुश्मन की फौजें आसपास तो नहीं, हम उनकी बैंड बजा देंगे.' तो वो झट से जवाब देता, ‘हाँ मासी, मैं अभी बैंडवाले को फोन करता हूँ.’ मैं उससे कहती 'हम दुश्मन को हराने की नयी रणनीति बनाएंगे', तो वो मुस्तैद जवाब देता, ‘वैसे मुझे मालूम नहीं है कि रणनीति होती क्या है, लेकिन हम बनायेंगे ज़रूर’ कितनी ही बार वो लम्हे याद करके मुस्कुराई हूँ.
तमाम कुर्सियों और चादर और बहुत सारी स्टिक्स की मदद से बने उस टेंट के अन्दर किये गये नाश्ते के स्वाद और अनि की शरारतों की खुशबू से अब तक सराबोर हूँ. उसकी हर अदा खूबसूरत है. विम्पीकिड की डायरी के लिए उसका दीवानापन, दीवारों पे टंगी उसकी पेंटिंग्स, उसकी तस्वीरों के पीछे की वो तमाम कहानियां जो उसने मुझे बताईं, साथ में मिट्टी के मटके बनाना सीखना, फिर उन्हें धूप में सुखाना, सुबह-सुबह ठंडी हवा में दुबक के खेलना ‘आई स्पाई....’
तमाम कुर्सियों और चादर और बहुत सारी स्टिक्स की मदद से बने उस टेंट के अन्दर किये गये नाश्ते के स्वाद और अनि की शरारतों की खुशबू से अब तक सराबोर हूँ. उसकी हर अदा खूबसूरत है. विम्पीकिड की डायरी के लिए उसका दीवानापन, दीवारों पे टंगी उसकी पेंटिंग्स, उसकी तस्वीरों के पीछे की वो तमाम कहानियां जो उसने मुझे बताईं, साथ में मिट्टी के मटके बनाना सीखना, फिर उन्हें धूप में सुखाना, सुबह-सुबह ठंडी हवा में दुबक के खेलना ‘आई स्पाई....’
प्यारे अनि, तुम जादूगर हो, तुम्हारे जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार तुमको, ढेर सारा दुलार, ढेर सारी मस्ती अभी भी उधार है...लव यू दोस्त...